आवरणकथा- तरुणाघातः हिल गए सिंहासन
संदीप कुमार
| 30 Sep 2025 |
176
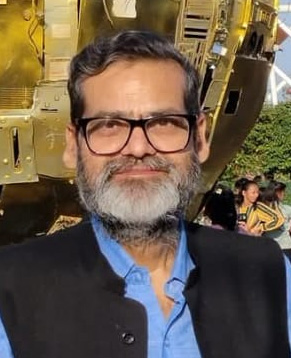

पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण एशिया की राजनीति ने एक ऐसा मोड़ लिया है, जिसकी पटकथा किसी पुराने नेता ने नहीं, बल्कि ‘जेन-ज़ेड’ ने लिखी है। बांग्लादेश की गलियों से लेकर श्रीलंका के समुद्रतटों और नेपाल की पहाड़ियों तक—युवा हाथों में प्लेकार्ड और मोबाइल लिए सड़कों पर उतर आए। नतीजा? दशकों से जमे सिंहासन हिल गए, और सत्ता के पुराने किले ढहने लगे। सत्ता और उसके समर्थकों ने कहा यह स्वस्फूर्त आंदोलन नहीं। इसमें बाहरी साजिश है जबकि बाकियों का कहना था कि इस नरेटिव की आड़ में सरकारें अपनी विफलता और भ्र्ष्टाचार छिपाना चहती हैं। यह आलेख इन्हीं उलझनों को सुलझाने की कोशिश करता है—इन आंदोलनों के असली कारणों, सोशल मीडिया और डिजिटल शक्ति की भूमिका, और वैश्विक ताक़तों के उस जटिल खेल को उजागर करते हुए, जो दक्षिण एशिया के भविष्य को तय करने जा रहा है।
पिछले कुछ वर्षों से दक्षिण एशिया का राजनीतिक परिदृश्य एक नए और अप्रत्याशित अध्याय का गवाह बन रहा है। दशकों तक सैन्य तख्तापलट या पारंपरिक चुनावी उलटफेर के आदी इस क्षेत्र में अब एक नई ताकत उभरी है: 'जेन-ज़ेड' । यह वह युवा पीढ़ी है, जिसने बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में सड़कों पर उतरकर सत्ता के पुराने समीकरणों को चुनौती दी, और कई मामलों में, उन्हें उखाड़ फेंका। यह सिर्फ़ एक क्षेत्रीय परिघटना नहीं, बल्कि 'अरब स्प्रिंग' की प्रतिध्वनि है, जिसकी जड़ें ईरानी क्रांति तक जा पहुँचती हैं – एक ऐसा ट्रेंड जहाँ जनता का आक्रोश, विशेषकर युवाओं का, अप्रत्याशित राजनीतिक परिवर्तन लाता है। लेकिन क्या ये आंदोलन सिर्फ़ घरेलू असंतोष का परिणाम हैं, या फिर पर्दे के पीछे से कोई 'ग्लोबल डीप स्टेट' अपने हितों के तहत इन ज्वलंत विद्रोहों को हवा दे रहा है? यह सवाल इस पूरे घटनाक्रम को एक जटिल भू-राजनीतिक पहेली में बदल देता है, जिसकी परतों को सावधानी से उधेड़ना आवश्यक है।
दक्षिण एशिया में 'स्प्रिंग' की आहट
श्रीलंका के 'अरगलय' से लेकर बांग्लादेश के 'द्वितीय मुक्ति' और नेपाल के 'जेन-ज़ेड विद्रोह' तक, इन आंदोलनों ने स्पष्ट कर दिया है कि दक्षिण एशिया में राजनीतिक अस्थिरता का एक नया दौर शुरू हो चुका है। प्रत्येक देश की अपनी विशिष्ट पृष्ठभूमि और तात्कालिक ट्रिगर थे, लेकिन इन सभी में एक गहरा और साझा असंतोष छिपा था: वादों के टूटने, भ्रष्टाचार के फैलाव और एक ऐसे राजनीतिक कुलीन वर्ग की अनदेखी के प्रति क्रोध, जिसने युवा पीढ़ी को एक अंधकारमय भविष्य की ओर धकेल दिया था।
श्रीलंकाः जब आर्थिक सुनामी ने राजवंश को डुबोया
2022 में श्रीलंका का 'अरगलय' (सिंहली में 'संघर्ष') आंदोलन सिर्फ़ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था; यह उस आर्थिक सुनामी का सीधा जवाब था, जिसने एक समय समृद्ध दिखने वाले द्वीप राष्ट्र को घुटनों पर ला दिया था। महीनों तक चली अभूतपूर्व मुद्रास्फीति, ईंधन और रसोई गैस के लिए अंतहीन कतारें, 12 घंटे की बिजली कटौती और आवश्यक वस्तुओं की गंभीर कमी ने दैनिक जीवन को नरक बना दिया था। इस आर्थिक संकट का सीधा आरोप राजपक्षे परिवार पर लगा, जिसने पिछले 18 में से 15 वर्षों तक देश पर शासन किया था। अर्थव्यवस्था के ढहने और दैनिक जीवन के असहनीय हो जाने पर यह आंदोलन तेज हुआ, जिससे गोटाबाया राजपक्षे जैसे वंशवादी नेताओं को सत्ता छोड़नी पड़ी। जनता का आक्रोश इस हद तक पहुँचा कि उन्होंने राष्ट्रपति गोताबया राजपक्षे के आलीशान निवास और कोलंबो में 'गोटा गो गामा' नामक विरोध स्थल को अपने नियंत्रण में ले लिया, जहाँ कला, संगीत और भाषणों के माध्यम से विरोध का एक अनूठा केंद्र विकसित हुआ। यह आंदोलन, जिसे युवा कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया के ज़रिए संगठित किया, गोताबया राजपक्षे को देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर गया। यह सिर्फ़ एक नेता का पतन नहीं था, बल्कि एक वंशवादी शासन का अंत था, जिसकी जड़ें देश की राजनीति में गहराई तक जम चुकी थीं। 'सिस्टम चेंज' की गूँज कोलंबो की सड़कों पर सुनाई देने लगी थी, जो सिर्फ़ नेताओं को बदलने से कहीं ज्यादा संस्थागत और संरचनात्मक सुधारों की आकांक्षा को दर्शाता। आंदोलन के पीछे विदेशी साजिश के दावों की पड़ताल में निर्णायक प्रमाण नहीं मिले। इसके बजाय, मानवाधिकार संगठनों ने इसे घरेलू विफलताओं और जनाक्रोश का परिणाम बताया।
बांग्लादेश का 'द्वितीय मुक्ति'
बांग्लादेश में 2024 का घटनाक्रम एक छात्र-नेतृत्व वाले अभियान के रूप में शुरू हुआ, जिसका निशाना सरकारी नौकरियों में 'भेदभावपूर्ण' कोटा प्रणाली थी। यह कोटा, जो 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गजों के वंशजों के लिए 30% तक सीटें आरक्षित करता था, युवा पीढ़ी को सीधे तौर पर अव्यवस्था और भाई-भतीजावाद का प्रतीक लगा। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस माँग का उपहास करते हुए छात्रों को 'राजकार' (पाकिस्तान के सहयोगी) कहा, जो एक ऐसा अपमान था जिसने विद्रोह को और भड़का दिया। छात्रों ने इस शब्द को 'बैज ऑफ़ ऑनर' की तरह पहना और 'कौन हो तुम? कौन हूँ मैं? राजकार। किसने कहा? तानाशाह!' जैसे नारे सड़कों पर गूँजने लगे। पुलिस की बर्बर कार्रवाई में सैकड़ों निर्दोष प्रदर्शनकारियों की मौत ने आंदोलन का चरित्र ही बदल दिया। यह अब सिर्फ़ कोटा के खिलाफ़ नहीं, बल्कि शेख हसीना के लंबे और सत्तावादी शासन के खिलाफ़ एक व्यापक विद्रोह बन गया, जिन्होंने 15 वर्षों से अधिक समय तक देश पर शासन किया था। उस युवा पीढ़ी के लिए, जिसने हसीना के शासन के अलावा कुछ देखा ही नहीं था, उनका शासन उत्पीड़न और अवसरों की कमी का पर्याय बन चुका था। सोशल मीडिया ने इस आंदोलन को एक ढीली संरचना और व्यापक पहुँच प्रदान की, और अंततः 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को देश छोड़कर भारत भागना पड़ा। नोबेल विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य देश को नए और निष्पक्ष चुनावों की ओर ले जाना था।बांग्लादेश की शासक पार्टी ने आंदोलकारी छात्रों पर पाकिस्तान या अमेरिकी हस्तक्षेप की अफवाहें जरूर चलाईं, लेकिन स्वतंत्र रिपोर्ट्स में आंदोलन की जड़ें देश की सामाजिक-आर्थिक असमानता और सत्ताधारी दल की अलोकप्रिय नीतियों तक ही सीमित रहीं।
नेपाल का 'जेन-जेड विद्रोह'
नेपाल में 2025 का आंदोलन एक तात्कालिक ट्रिगर से शुरू हुआ: सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाया गया प्रतिबंध, जिसे 'गलत इस्तेमाल' और 'पंजीकरण' न करने का हवाला देकर लागू किया गया था। लेकिन यह प्रतिबंध सिर्फ़ चिंगारी थी। दशकों से पनप रही असमानता, व्यापक भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और राजनीतिक कुलीन वर्ग के हाथों में सिमटी सत्ता ने युवा पीढ़ी में गहरे असंतोष को जन्म दिया था। #NepoKid जैसे सोशल मीडिया ट्रेंड्स ने राजनेताओं के बच्चों की विलासितापूर्ण जीवनशैली और विदेशी शिक्षा को उजागर किया, जबकि देश का युवा बेरोजगारी और पलायन की मार झेल रहा था। यह 'नैतिक आक्रोश' था, जैसा कि विश्लेषक कहते हैं, एक पीढ़ी के खिलाफ़ जिसने उनका भविष्य चुरा लिया था। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने शुरू में आंदोलनकारियों का उपहास किया, लेकिन जब विरोध प्रदर्शन हिंसक हो उठे, 70 से अधिक लोग मारे गए और संसद भवन व उनके अपने घर पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया, तो ओली को इस्तीफा देना पड़ा। हिंसा के बावजूद, युवाओं की इस आवाज़ को दबाया नहीं जा सका। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, जिनकी नियुक्ति में युवा-नेतृत्व वाले ऑनलाइन सर्वेक्षण ने भी भूमिका निभाई थी, जो 'डिजिटल लोकतंत्र' के एक नए रूप का प्रतीक था। नेपाल में जेन ज़ेड आंदोलन के युवा आंदोलनकारियों की मुख्य मांगें ‑ भ्रष्टाचार का खात्मा, पारदर्शी और जवाबदेह शासन तथा सोशल मीडिया पर से बैन हटाना थीं। सरकार और कुछ समर्थकों ने इसे विदेशी साजिश कहने की कोशिश की, लेकिन आंदोलन को नेतृत्व देने वालों, मानवाधिकार पर्यवेक्षकों और अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों ने इसे स्थानीय असंतोष और असफल शासन व्यवस्था का परिणाम माना है। कई जगह सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं और बाहरी प्रभाव की अफवाहें जरूर आईं, लेकिन प्रमाण ऐसे नहीं मिले कि आंदोलन मुख्यतः विदेशी साजिश थी
पीढ़ीगत खाई और ध्वस्त होती उम्मीदें
इन सभी आंदोलनों के पीछे कुछ गहरे संरचनात्मक मुद्दे हैं, जो दक्षिण एशिया की युवा आबादी के लिए एक अनिश्चित भविष्य की तस्वीर पेश करते हैं। सत्ता पक्ष ने शुरू में या तो विदेशी साजिश, या विपक्षी दलों की मिलीभगत के आरोप लगाए, परंतु स्थापित पत्रकारों, शोधकर्ताओं और मानवाधिकार संगठनों का निष्कर्ष यही है कि आंदोलनों की वजह— भ्रष्टाचार, आर्थिक असफलताएं, बेरोजगारी और अलोकतांत्रिक प्रवृत्तियां थीं। डिजिटल माध्यमों ने युवाओं की नाराजगी को नया मंच दिया, और सरकारों के दावों के बावजूद, आंदोलन व्यापक घरेलू असंतोष के प्रतीक बने।
अवसरहीनता का दलदल और आर्थिक कुप्रबंधन
दक्षिण एशिया एक युवा क्षेत्र है, जहाँ इन तीनों देशों की लगभग 50% आबादी 28 वर्ष से कम है। उनकी साक्षरता दर 70% से अधिक है, लेकिन प्रति व्यक्ति जीडीपी वैश्विक औसत से काफ़ी कम है। इस शैक्षिक योग्यता और आर्थिक अवसर के बीच का विशाल अंतर ही आक्रोश का मूल है। श्रीलंका में 22.3%, बांग्लादेश में 16.8% और नेपाल में 20.8% की युवा बेरोजगारी दर एक विस्फोटक मिश्रण तैयार करती है। यह वह पीढ़ी है जिसने अपने जीवनकाल में कम से कम दो बड़ी आर्थिक मंदी (2008-09 और COVID-19) का अनुभव किया है। उन्हें लगता है कि उनकी क्षमता और आकांक्षाओं को राजनीतिक व्यवस्था ने रौंद दिया है, जिससे 'ब्रेन ड्रेन' की समस्या गंभीर हो गई है, जहाँ लाखों युवा बेहतर अवसरों की तलाश में विदेशों में पलायन कर रहे हैं। नेपाल की अर्थव्यवस्था का एक तिहाई हिस्सा रेमीटेंस पर निर्भर करता है, जो इस पलायन की भयावहता को दर्शाता है। यह सिर्फ़ आर्थिक निर्णय नहीं, बल्कि सरकार की अक्षमता पर 'मौन जनमत संग्रह' है।
भ्रष्टाचार का दीमक और भाई-भतीजावाद की बेल
इन देशों में भ्रष्टाचार का स्तर इतना गहरा है कि इसने सार्वजनिक जीवन के हर पहलू को खोखला कर दिया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में उनकी खराब रैंकिंग (सभी 100 से ऊपर) एक गंभीर संस्थागत विफलता को उजागर करती है। सरकारी कार्यालयों में रिश्वतखोरी, सरकारी ठेकों और टेंडरों में मनमानी, तथा सरकारी नौकरियों में 'अपने लोगों' को प्राथमिकता देना आम बात हो गई है। #NepoKid आंदोलन ने इस भाई-भतीजावाद को सीधे युवाओं के गुस्से का निशाना बनाया। जब राजनीतिक कुलीन वर्ग के बच्चे विदेशों में विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं, जबकि आम युवा नौकरी के लिए तरसते हैं, तो यह नैतिक आक्रोश एक ज्वलनशील स्थिति पैदा करता है। सुमन पांडे, नेपाल के पर्यटन उद्योग के एक अनुभवी व्यक्ति, ने इसे 'माफिया' शासन बताया, जहाँ 'पिछले 30 सालों से तीन लोगों के बीच म्यूजिकल चेयर्स का खेल चल रहा था और उन्होंने युवा राजनेताओं को कभी मौका नहीं दिया।'
सत्ता का क्षरण और संवादहीनता
इन आंदोलनों का एक मार्मिक पहलू नेताओं की उम्र और युवा प्रदर्शनकारियों की उम्र के बीच का बड़ा अंतर है। नेपाल के ओली 73, बांग्लादेश की हसीना 76 और श्रीलंका के राजपक्षे 74 वर्ष के थे। मीनाक्षी गांगुली, ह्यूमन राइट्स वॉच की उप-एशिया निदेशक, कहती हैं, 'दक्षिण एशिया में युवा अपने राजनीतिक नेताओं से जुड़ने के लिए कुछ भी नहीं ढूँढ पा रहे हैं। बेमेल बहुत ज़्यादा था।' यह बेमेल केवल आयु का नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं, दृष्टिकोणों और मूल्यों का भी था। पुराने नेता अक्सर अपनी विरासत और पिछले संघर्षों पर ध्यान केंद्रित करते थे, जबकि युवा भविष्य, अवसरों और न्याय पर केंद्रित थे। पारंपरिक राजनीतिक दल, जो अक्सर व्यक्ति-केंद्रित और गुटबाज़ी का शिकार होते थे, युवाओं की आकांक्षाओं को समझने या उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल करने में विफल रहे।
डिजिटल सशक्तिकरण: प्रतिरोध का नया अखाड़ा
जेन-जेड एक ऐसी पीढ़ी है जो इंटरनेट पर पली-बढ़ी है, और उनके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म सिर्फ़ मनोरंजन के साधन नहीं, बल्कि समुदाय, संगठन और आत्म-अभिव्यक्ति के शक्तिशाली उपकरण हैं। सोशल मीडिया ने इन आंदोलनों को संगठित करने, संदेश फैलाने और व्यापक समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हैशटैग अभियान जैसे #GoHomeGota और #NepoKid ने विरोध को एक एकीकृत आवाज़ दी। लाइव स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन संचार ने प्रदर्शनकारियों को वास्तविक समय में जुड़ने में मदद की और सरकार के दमनकारी प्रयासों को दुनिया के सामने उजागर किया। जब सरकारों ने इंटरनेट एक्सेस या विशिष्ट प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने की कोशिश की, तो इसका उल्टा असर हुआ और यह युवाओं के गुस्से को और भड़काने वाला साबित हुआ। डिजिटल तकनीक ने इन आंदोलनों को 'नेताविहीन' और विकेंद्रीकृत बनाए रखने में मदद की, जिससे पारंपरिक दमनकारी रणनीतियों के खिलाफ़ एक नया लचीलापन पैदा हुआ।
एक-दूसरे से प्रेरित होते विद्रोह
इन आंदोलनों ने एक-दूसरे से प्रेरणा ली है, और 'डिजिटल विरोध पुस्तिका' का विकास किया है। नेपाली युवाओं ने श्रीलंका और बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शनों को करीब से देखा और उनसे सीखा। कोलंबिया विश्वविद्यालय की रुमेला सेन कहती हैं कि इन आंदोलनों में इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति, 'जिसमें सोशल मीडिया पर हैशटैग अभियान और विकेन्द्रीकृत संगठन शामिल हैं, डिजिटल विरोध के एक उभरते हुए प्लेबुक का प्रतिनिधित्व करते हैं।' यह क्षेत्रीय एकीकरण, हालांकि अनौपचारिक है, एक शक्तिशाली संकेत है कि युवा पीढ़ी अपनी समस्याओं को अलग-थलग घटनाओं के रूप में नहीं देखती, बल्कि एक व्यापक पैटर्न के हिस्से के रूप में देखती है।
'ग्लोबल डीप स्टेट' की छाया?
इन व्यापक जन आंदोलनों के उभार के साथ ही, एक विवादास्पद अवधारणा – 'ग्लोबल डीप स्टेट' – की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। यह परिकल्पना, जो अक्सर षड्यंत्र-सिद्धांतों से जुड़ी होती है, मानती है कि वैश्विक स्तर पर कुछ शक्तिशाली, अप्रत्यक्ष अभिनेता (राज्य या गैर-राज्य) अपने भू-राजनीतिक और आर्थिक हितों को साधने के लिए विभिन्न संगठनों और माध्यमों से सत्ता परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। यह तर्क दिया जाता है कि ये शक्तियाँ अरब स्प्रिंग से लेकर उससे पहले की ईरानी क्रांति तक के आंदोलनों में सक्रिय रही हैं। दक्षिण एशिया के इन युवा-नेतृत्व वाले विद्रोहों में भी कुछ लोग बाहरी ताकतों के हाथ होने का आरोप लगाते हैं, विशेषकर जब सत्ता परिवर्तन इतनी तेज़ी से होता है कि स्थानीय लोगों को भी विश्वास नहीं होता।
'डीप स्टेट' की अवधारणा का अनावरण
'डीप स्टेट' शब्द आम तौर पर किसी देश के भीतर एक समानांतर, अप्रत्यक्ष सत्ता संरचना को संदर्भित करता है जो निर्वाचित सरकार से स्वतंत्र रूप से काम करता है, अक्सर खुफिया एजेंसियों, सैन्य प्रतिष्ठानों और शक्तिशाली नौकरशाहों के माध्यम से। 'ग्लोबल डीप स्टेट' इस अवधारणा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित करता है, जहाँ शक्तिशाली देशों की खुफिया एजेंसियां, बहुराष्ट्रीय निगम, थिंक टैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं और वैश्विक गैर-सरकारी संगठन पर्दे के पीछे से काम करते हैं। उनका उद्देश्य राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना, सरकारों को कमजोर करना, या ऐसे सत्ता परिवर्तन को सुविधाजनक बनाना हो सकता है जो उनके रणनीतिक या आर्थिक लाभ के लिए फायदेमंद हो। ये हस्तक्षेप अक्सर 'लोकतंत्र को बढ़ावा देने', 'मानवाधिकारों की रक्षा करने' या 'स्थिरता स्थापित करने' के आवरण में छिपे होते हैं, लेकिन आलोचक इसे बाहरी शक्तियों द्वारा अपने भू-राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने का एक मुखौटा मानते हैं।

दक्षिण एशिया के मोर्चे पर बाहरी हस्तक्षेप के स्वर
इन दक्षिण एशियाई मामलों में, बाहरी ताकतों की भूमिका को लेकर आरोप और प्रत्यारोप सुनाई देते रहे हैं। लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बाहरी अभिनेता शायद ही कभी शून्य से जन आंदोलनों को उत्पन्न करते हैं। इसके बजाय, वे मौजूदा घरेलू कमजोरियों, असंतोष और संस्थागत दरारों का लाभ उठाते हैं।
भारत और नेपाल का जटिल रिश्ता: नेपाल की अस्थिरता का भारत पर तत्काल और सीधा सुरक्षा प्रभाव पड़ता है। खुली सीमा और गहरे ऐतिहासिक-सांस्कृतिक संबंधों के कारण, भारत काठमांडू में एक स्थिर और विश्वसनीय साझेदार चाहता है। नेपाली वामपंथी और राजशाही समर्थक अक्सर भारत पर अपनी राजनीति में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते रहे हैं। केपी शर्मा ओली की चीन-उन्मुख नीतियों ने निश्चित रूप से भारत को असहज किया होगा। ओली सरकार के पतन के बाद भारत द्वारा अंतरिम सरकार का तुरंत स्वागत करना इस बात का संकेत हो सकता है कि दिल्ली ने इस बदलाव को अपने पक्ष में देखा।
चीन की बढ़ती रणनीतिक पैठ: नेपाल की उत्तरी सीमा चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से लगती है, और बीजिंग ने हाल के वर्षों में नेपाल में अपना कूटनीतिक और आर्थिक प्रभाव बढ़ाया है। चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नेपाल को 'ट्रांस-हिमालयन नेटवर्क' का हिस्सा बनाना चाहती है, जिसे भारत अक्सर चीन की विस्तारवादी रणनीति के रूप में देखता है। नेपाल की वामपंथी पार्टियों का चीन की ओर झुकाव स्पष्ट है। ओली का बीजिंग सैन्य परेड में भाग लेना और लिपुलेख दर्रे पर भारत-चीन समझौते पर आपत्ति जताना, चीन के साथ उनकी बढ़ती निकटता को दर्शाता था। चंद्र भट्ट जैसे भू-राजनीतिक विश्लेषक इसे 'असामान्य' बताते हैं, क्योंकि नेपाल का जुड़ाव पारंपरिक रूप से भारत और पश्चिम से अधिक रहा है।
पश्चिम का 'लोकतांत्रिक' प्रभाव: अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे पश्चिमी देश अक्सर वित्तपोषण के माध्यम से नेपाल में नीतिगत ढाँचों और नागरिक समाज का समर्थन करते हैं। अमेरिका द्वारा मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन के तहत नेपाल में पावर ग्रिड और सड़क ढांचे के लिए 530 मिलियन डॉलर का अनुदान, जिसे अक्सर चीन के BRI के जवाब के रूप में देखा जाता है, पश्चिमी देशों के रणनीतिक हितों को दर्शाता है। श्रीलंका में 'अरगलय' के दौरान, कुछ अति-राष्ट्रवादियों ने USAID पर विरोध प्रदर्शनों को वित्तपोषित करने का आरोप लगाया, हालांकि इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिले। पश्चिमी हित अक्सर लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकारों और सुशासन के नाम पर काम करते हैं, जिसे 'डीप स्टेट' के सिद्धांतकार बाहरी हस्तक्षेप का एक रूप मानते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का दबाव: श्रीलंका के आर्थिक संकट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की भूमिका उल्लेखनीय थी। IMF के साथ किसी भी बचाव पैकेज के लिए अक्सर कठोर आर्थिक सुधारों और मितव्ययिता उपायों को लागू करने की शर्त रखी जाती है, जो अल्पावधि में जनता के असंतोष को बढ़ा सकते हैं। हालांकि IMF सीधे तौर पर सत्ता परिवर्तन को बढ़ावा नहीं देता, इसकी नीतियां अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक अस्थिरता को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे बाहरी शक्तियों के लिए 'प्रबंधन' के अवसर पैदा हो सकते हैं।
भू-राजनीतिक शक्तियों का बारीक खेल: यह तर्क देना अधिक यथार्थवादी है कि इन दक्षिण एशियाई आंदोलनों का प्राथमिक चालक गहरी घरेलू शिकायतें और संस्थानों की विफलता है। बाहरी शक्तियाँ शायद ही कभी जन आंदोलनों को शून्य से उत्पन्न करती हैं; इसके बजाय, वे मौजूदा असंतोष, आर्थिक संकट और कमजोर शासन का लाभ उठाने के लिए तैयार रहती हैं। नेपाल में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का बधाई संदेश या जापान का ओली के पतन पर तुरंत स्वागत करना, बाहरी अभिनेताओं द्वारा 'पसंद' किए गए परिणामों के संकेतक हो सकते हैं, न कि सीधे उकसावे के।
भू-राजनीतिक शक्तियाँ अक्सर 'सूचना युद्ध' और 'नैरेटिव निर्माण' में संलग्न होती हैं, जहाँ सोशल मीडिया एक प्रमुख युद्ध का मैदान बन जाता है। वे विरोध प्रदर्शनों को बढ़ावा देने, एक विशेष परिणाम के लिए सार्वजनिक राय को प्रभावित करने या अपने अनुकूल नैरेटिव स्थापित करने के लिए लक्षित प्रचार का उपयोग कर सकते हैं। यह 'सॉफ्ट पावर' का खेल है, जहाँ विचारों और सूचनाओं के माध्यम से प्रभाव डाला जाता है।
सैन्य संस्थानों की भूमिका भी इस भू-राजनीतिक समीकरण में महत्वपूर्ण है। श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, तीनों देशों में सैन्य ने सरकार परिवर्तन के दौरान एक निश्चित संयम दिखाया। श्रीलंका में सेना ने प्रदर्शनकारियों पर सीधे बल प्रयोग से परहेज किया और राजपक्षे को सुरक्षित निकलने में मदद की। बांग्लादेश और नेपाल में भी सैन्य ने एक 'किंगमेकर' की भूमिका निभाई, जिससे एक सुचारू (हालांकि अनिश्चित) संक्रमण सुनिश्चित हुआ। यह संयम आंतरिक मूल्यांकन का परिणाम हो सकता है, लेकिन यह बाहरी शक्तियों के साथ समझ या दबाव का भी परिणाम हो सकता है, जो अराजकता के बजाय क्षेत्रीय स्थिरता पसंद करते हैं, क्योंकि पूर्ण अराजकता उनके निवेश और रणनीतिक हितों के लिए अधिक हानिकारक होती है।
संक्षेप में, यह अधिक संभावना है कि बाहरी अभिनेता इन आंदोलनों को 'मैनेज' या 'नेविगेट' करने का प्रयास करते हैं, बजाय इसके कि वे उन्हें 'रचना' करें। उनका उद्देश्य अक्सर अपने दीर्घकालिक हितों के अनुरूप एक अनुकूल परिणाम सुनिश्चित करना होता है, जो अक्सर स्थिरता, आर्थिक पहुंच और भू-राजनीतिक संतुलन से जुड़ा होता है। वे मौजूदा समस्याओं को बढ़ाने में निवेश कर सकते हैं, लेकिन उन समस्याओं को उत्पन्न करने में नहीं, जो पहले से ही घरेलू परिस्थितियों में मौजूद हैं।
अराजकता या नया सवेरा?
इन युवा-नेतृत्व वाले आंदोलनों के परिणाम तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों हैं, जिनमें भारी अनिश्चितता और नई चुनौतियाँ भी शामिल हैं। प्रधानमंत्रियों के इस्तीफ़े और अंतरिम सरकारों की स्थापना तो हो गई है, लेकिन असली संघर्ष अब शुरू होता है।
सत्ता का शून्य और अवसरवादियों की दस्तक: 'नेताविहीन' प्रकृति के बावजूद, इन आंदोलनों ने अक्सर एक राजनीतिक शून्य पैदा किया, जिसे विभिन्न राजनीतिक दल और अवसरवादी समूह भरने की कोशिश करते हैं। श्रीलंका में, वामपंथी जनथा विमुक्ति पेरामुना के नेतृत्व वाले नेशनल पीपल्स पावर गठबंधन ने 'अरगलय' की ऊर्जा का सफलतापूर्वक लाभ उठाया और 2024 के चुनावों में भारी जीत हासिल की। यह दर्शाता है कि कैसे एक लोक-लुभावन आंदोलन एक स्थापित राजनीतिक दल के लिए सत्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, भले ही वह दल पहले हाशिए पर रहा हो। बांग्लादेश में, जमात-ए-इस्लामी समर्थित संगठनों की विश्वविद्यालय चुनावों में जीत एक चिंताजनक प्रवृत्ति को रेखांकित करती है, जहाँ कट्टरपंथी विचारधाराएँ राजनीतिक शून्य का लाभ उठाकर उभर सकती हैं। नेपाल में भी, नए युवा-आधारित राजनीतिक दलों के गठन की बात हो रही है, लेकिन पुराने दल भी नए चेहरों के साथ वापसी की फिराक में हैं।
संस्थागत सुधारों की अनवरत चुनौती: आंदोलन भले ही तत्काल सत्ता परिवर्तन ला दें, लेकिन स्थायी संस्थागत सुधारों को लागू करना कहीं अधिक कठिन और लंबा संघर्ष है। श्रीलंका में, राजपक्षे राजवंश को उखाड़ फेंका गया, लेकिन संस्थागत भ्रष्टाचार और जवाबदेही की समस्या अभी भी बनी हुई है। NPP सरकार, जिसने बदलाव का वादा किया था, को भी IMF समझौतों और आर्थिक चुनौतियों के बीच कठोर निर्णय लेने पड़ रहे हैं, जो उसके चुनावी वादों से भिन्न हो सकते हैं। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार को लंबे समय से चली आ रही सत्तावादी प्रणालियों, राजनीतिक ध्रुवीकरण और अल्पसंख्यकों के खिलाफ़ हिंसा की चुनौतियों से निपटना पड़ रहा है। नेपाल में भी, अंतरिम सरकार को पिछली सरकार के भ्रष्ट तत्वों के खिलाफ़ कार्रवाई करने और मुक्त व निष्पक्ष चुनाव कराने की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
युवाओं की बेसब्र उम्मीदें और क्षेत्रीय स्थिरता: अंतरिम सरकारों को जनता, विशेषकर युवाओं के विश्वास को बहाल करना होगा, जिनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ़ कार्रवाई करनी होगी, आर्थिक स्थिरता लानी होगी और सबसे महत्वपूर्ण, रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने होंगे। यदि वे इन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, तो निराशा का एक नया चक्र शुरू हो सकता है, जिससे और अधिक विरोध प्रदर्शनों की संभावना बढ़ जाएगी।
क्षेत्रीय स्तर पर, एक देश में राजनीतिक अस्थिरता का दूसरे देशों पर 'छूने' का प्रभाव हो सकता है, जिससे पूरे क्षेत्र में इसी तरह के आंदोलनों को बढ़ावा मिल सकता है। यह 'दक्षिण एशिया के लिए एक नया डॉक्टरिन ऑफ इन्स्टेबिलिटी' बन सकता है, जहाँ युवा आक्रोश एक देश से दूसरे देश में फैल सकता है। यह बाहरी शक्तियों को भी अपनी भू-राजनीतिक रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करेगा। भारत, चीन और अमेरिका जैसे देश अपने हितों की रक्षा के लिए अपनी कूटनीतिक और आर्थिक सहायता में बदलाव कर सकते हैं।
चौराहे पर दक्षिण एशिया
दक्षिण एशिया में जेन-जेड के नेतृत्व वाले सत्ता परिवर्तन आंदोलन डिजिटल युग के 'पब्लिक स्फीयर' का एक स्पष्ट उदाहरण हैं, जहाँ सोशल मीडिया ने सत्ता-विरोधी भावनाओं को एक साझा मंच दिया है। ये विद्रोह घरेलू असंतोष, आर्थिक कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और राजनीतिक कुलीन वर्ग से युवाओं के गहरे मोहभंग का सीधा परिणाम हैं। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि युवा पीढ़ी अपने भविष्य को पुराने राजनीतिक समीकरणों के हाथों में छोड़ने को तैयार नहीं है।
बड़ी तस्वीर में दो तरह की संभावनाएँ हैं। एक सकारात्मक दिशा यह है कि यदि ये आंदोलन स्थायी संस्थागत सुधार लाने में सफल होते हैं – जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशी शासन शामिल है – तो दक्षिण एशिया लोकतंत्र और विकास के एक नए युग में प्रवेश कर सकता है। श्रीलंका में NPP की जीत और बांग्लादेश व नेपाल में अंतरिम सरकारों का गठन, यदि वे सही दिशा में काम करते हैं, तो एक नई शुरुआत का संकेत हो सकते हैं। दूसरी तरफ, एक नकारात्मक दिशा यह हो सकती है कि यदि यह ऊर्जा सिर्फ़ 'सत्ता पलट' तक ही सीमित रही और ठोस संस्थागत सुधार नहीं हुए, तो पैदा हुआ राजनीतिक शून्य नए अवसरवादियों, कट्टरपंथियों और अलोकतांत्रिक शक्तियों से भर जाएगा, जिससे अस्थिरता का चक्र और भी गहराएगा।
यह भी स्पष्ट है कि 'ग्लोबल डीप स्टेट' इन घटनाओं को उकसाता नहीं, बल्कि इन्हें अपने हित में इस्तेमाल करता है। बाहरी शक्तियों का उद्देश्य अराजकता फैलाना नहीं, बल्कि उसे इस तरह से प्रबंधित करना है ताकि परिणाम उनके पक्ष में झुके। वे मौजूदा घरेलू दरारों का लाभ उठाते हैं, सूचना युद्ध में संलग्न होते हैं, और संकट को अपने भू-राजनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप ढालने की कोशिश करते हैं। सैन्य संस्थानों का 'संयमित' व्यवहार अक्सर इसी बड़े भू-राजनीतिक प्रबंधन का हिस्सा होता है, जो कुल मिलाकर अराजकता को रोककर क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। इसलिए, विदेशी साजिश वाली दलीलें अधिकतर सरकारों की अपनी जिम्मेदारी और विफलता से ध्यान हटाने की कोशिश प्रतीत होती हैं। इन देशों में स्पष्ट रूप से सामने आया कि युवाओं का आक्रोश लोकल कारणों से शुरू हुआ और उसकी मूल वजह भ्रष्टाचार, सरकार की विफलता और लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण थी— न कि कोई बाहरी साजिश
अंततः, दक्षिण एशियाई सरकारों के लिए यह एक सीधा और स्पष्ट संदेश है कि सिर्फ़ चुनाव और सत्ता का प्रतीकात्मक हस्तांतरण अब पर्याप्त नहीं है। उन्हें पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना होगा, युवाओं को सार्थक रोजगार और आर्थिक अवसर प्रदान करने होंगे, शिक्षा प्रणाली को बाज़ार की ज़रूरतों से जोड़ना होगा, और आर्थिक सुधारों को जनता-उन्मुख बनाना होगा। अन्यथा, शिक्षा का ज्ञान, बेरोज़गारी का दर्द और डिजिटल माध्यमों की शक्ति मिलकर लगातार नई बगावतें पैदा करते रहेंगे। जेन-ज़ेड ने एजेंडा तय कर दिया है। अब यह क्षेत्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वह इस ज्वलंत ऊर्जा को स्थायी और सकारात्मक दिशा देता है, या इसे अराजकता के चक्र में फिर से खो जाने देता है। दक्षिण एशिया एक महत्वपूर्ण चौराहे पर खड़ा है, जहाँ भविष्य का मार्ग उसकी अपनी चुनी हुई राह पर ही निर्भर करेगा।